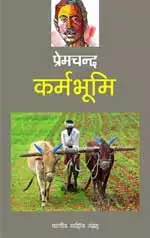|
उपन्यास >> कर्मभूमि (उपन्यास) कर्मभूमि (उपन्यास)प्रेमचन्द
|
31 पाठक हैं |
प्रेमचन्द्र का आधुनिक उपन्यास…
सुखदा कातर कण्ठ से बोली–‘आप अब क्यों नहीं चले जातें?’
समरकान्त ने नाक सिकोड़कर कहा–‘मैं क्यों जाऊँ, अपने कर्मों का फल भोगे। वह लड़की जो थी, सकीना, उसकी शादी की बातचीत उसी दुष्ट सलीम से हो रही है, जिसने लालाजी को गिरफ़्तार किया है। अब आँखें ख़ुली होंगी।’
सुखदा ने सहृदयता से भरे हुए स्वर में कहा–‘आप तो उन्हें कोस रहे हैं दादा। वास्तव में दोष उनका न था। सरासर मेरा अपराध था। उनका–सा तपस्वी पुरुष मुझ-जैसी विलासिनी के साथ कैसे प्रसन्न रह सकता था, बल्कि यों कहों कि दोष न मेरा था, न आपका, न उनका, सारा विष लक्ष्मी ने बोया। आपके घर में उनके लिए स्थान न था। आप उनसे बराबर खिंचे रहते थे। मैं भी उसी जलवायु में पली थी। उन्हें न पहचान सकी। वह अच्छा या बुरा जो कुछ करते थे, घर में उनका विरोध होता था। बात-बात पर उनका अपमान किया जाता था। ऐसी दशा में कोई भी सन्तुष्ट न रह सकता था। मैंने यहाँ एकान्त में इस प्रश्न पर खूब विचार किया है और मुझे अपना दोष स्वीकार करने में लेशमात्र भी संकोच नहीं है। आप एक क्षण भी यहाँ न ठहरें। वहाँ जाकर अधिकारियों से मिले, सलीम से मिलें और उनके लिए कुछ हो सके, करे। हमने उनकी विशाल तपस्वी आत्मा को भोग के बन्धनों से बाँधकर रखना चाहा था। आकाश में उड़ने वाले पक्षी को पिजड़े में बन्द करना चाहते थे। जब पक्षी पिंजड़े को तोड़कर उड़ गया, तो मैंने समझा। मैं अभागिनी हूँ। आज मुझे मालूम हो रहा है, वह मेरा परम सौभाग्य था।’
समरकान्त एक क्षण तक चकित नेत्रों, से सुखदा की ओर ताकते रहे, मानो अपने कानों पर विश्वास न आ रहा हो। इस शीतल क्षमा ने जैसे उनके मुरझाये हुए पुत्र-स्नेह को हरा कर दिया। बोल–‘इसकी तो मैंने खूब जाँच की, बात कुछ नहीं थी। उस पर क्रोध था, उसी क्रोध में जो कुछ मुँह में आ गया, बक गया। वह ऐब उसमें कभी न था; लेकिन उस वक़्त मैं भी अन्धा हो रहा था। फिर मैं कहता हूँ, मिथ्या नहीं, सत्य ही सही, सोलहों आने सत्य सही, तो क्या संसार में जितने ऐसे मनुष्य हैं, उनकी गरदन मार दी जाती है? मैं बड़े-बड़े व्यभिचारियों के सामने मस्तक नवाता हूँ। तो फिर अपने घर में और उन्हीं के ऊपर जिनसे किसी प्रतिकार की शंका नहीं, धर्म और सदाचार का सारा भार लाद दिया जाये? मनुष्य पर जब प्रेम का बन्धन नहीं होता, तभी वह व्यभिचार करने लगता है। भिक्षुक द्वार-द्वार इसीलिए जाता है कि एक द्वार से उसकी क्षुधा-तृप्ति नहीं होती। अगर इसे दोष भी मान लूँ, तो ईश्वर ने क्यों निर्दोष संसार नहीं बनाया? जो कहो कि ईश्वर की इच्छा ऐसी नहीं है, तो मैं पूछूँगा, जब सब ईश्वर के अधीन है, तो वह मन को ऐसा क्यों बना देता है कि उसे किसी टूटी झोंपड़ी की भाँति बहुत-सी थूनियों से सँभालना पड़े। यहाँ तो ऐसा ही है, जैसे किसी रोगी से कहा जाय कि तू अच्छा हो जा। अगर रोगी में इतनी सामर्थ्य होती, तो वह बीमार ही क्यों पड़ता।’
एक ही साँस में अपने हृदय का सारा मालिन्य उँड़ेल देने के बाद लालाजी दम लेने के लिए रुक गये। जो कुछ इधर-उधर लगा–चिपटा रह गया हो, शायद उसे भी खुरचकर निकाल देने का प्रयत्न कर रहे थे।
|
|||||


 i
i