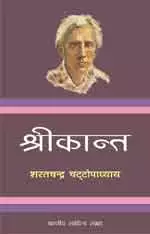|
उपन्यास >> श्रीकान्त श्रीकान्तशरत चन्द्र चट्टोपाध्याय
|
337 पाठक हैं |
शरतचन्द्र का आत्मकथात्मक उपन्यास
यथा-स्थान पहुँचकर देखा कि सरकी के झुण्ड के नीचे, उसी छोटी-सी नाव के ऊपर, इन्द्र सिर ऊपर उठाए मेरी राह देख रहा है। आँख से आँख मिलते ही उसने इस तरह हँसकर मुझे बुलाया कि न जाने की बात अपने मुँह से मैं निकाल ही न सका। सावधानी से, धीरे-धीरे उतरकर, चुपचाप, मैं नाव पर चढ़ गया। इन्द्र ने नाव खोल दी।
आज मैं सोचता हूँ कि बहुत जन्म के पुण्यों का फल था जो उस दिन मैं भय के मारे लौट न आया। उस दिन को उपलक्ष्य करके जो चीज मैं देख आया, उसे देखना, सारे जीवन सारी पृथ्वी छान डालने पर भी कितने से लोगों के भाग्य में होता है? स्वयं मैं भी वैसी वस्तु और कहाँ देख सका हूँ? जीवन में ऐसा शुभ मुहूर्त अनेक बार नहीं आता। यदि कभी आता भी है तो, वह समस्त चेतना पर ऐसी गम्भीर छाप मार जाता है कि बाद का सारा जीवन मानो उसी साँचे में ढल जाता है। मैं समझता हूँ कि इसीलिए मैं स्त्री-जाति को कभी तुच्छ रूप में नहीं देख सका। इसीलिए बुद्धि से मैं इस प्रकार के चाहे जितने तर्क क्यों न करूँ कि संसार में क्या पिशाचियाँ नहीं हैं? यदि नहीं, तो राह घाट में इतनी पाप-मूर्तियाँ किनकी देख पड़ती हैं? सब ही यदि इन्द्र की जीजी हैं, तो इतने प्रकार के दु:खों के स्रोत कौन बहाती हैं? तो भी, न जाने क्यों, मन में आता है कि यह सब उनके बाह्य आवरण हैं, जिन्हें कि वे जब चाहें तब दूर फेंककर ठीक उन्हीं के (दीदी के) समान उच्च आसन पर जाकर विराज सकती हैं। मित्र लोग कहते हैं कि यह मेरा अति जघन्य शोचनीय भ्रम है। मैं इसका भी प्रतिवाद नहीं करता, सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि यह मेरी युक्ति नहीं है, संस्कार है! इस संस्कार के मूल में जो है, नहीं मालूम, वह पुण्यवती आज भी जीवित है या नहीं। यदि हो भी तो वह कैसे, कहाँ पर है, इसकी खोज-खबर लेने की चेष्टा भी मैंने नहीं की है। किन्तु फिर भी मन ही मन मैंने उन्हें कितनी बार प्रणाम किया है, इसे भगवान ही जानते हैं।
|
|||||


 i
i