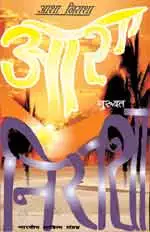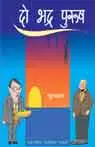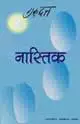|
उपन्यास >> आशा निराशा आशा निराशागुरुदत्त
|
203 पाठक हैं |
जीवन के दो पहलुओं पर आधारित यह रोचक उपन्यास...
‘‘न महात्मा गाँधी ने पाकिस्तान का विरोध करने के लिए शक्ति संचय की और न ही जवाहर लाल ने इस सीमा रेखाओं की रक्षा के लिए तैयारी की। मैं समझती हूं कि इस तैयारी के लिए कोई नैतिक आधार रह ही नहीं गया। यदि मुसलमानों के विशेषाधिकार स्वीकार न किये होते तो उनकी पृथक् देश की आवश्यकता पर विरोध युक्ति-युक्त होता। इसी प्रकार तिब्बत स्वतन्त्र होता तो भारत और तिब्बत में हुए समझौते का मान करने वाला कोई होता।
‘‘सन् १९१४ में चीन भारत से दुर्बल देश था। प्रथम विश्व युद्ध के उपरान्त चीन अपनी शक्ति संचय करने लगा। सन् १९४२ में चीन मित्र राष्ट्रों से मिल सका था। भारत को भी युद्ध में सम्मिलित हो कुछ सीखने का निमन्त्रण दिया गया था, परन्तु गाँधी जैसे ज्ञानहीन नेता भारत के नेताओं को इस ज्ञान से वंचित रखने में लीन थे। परिणाम यह हुआ कि युद्ध उपरान्त जहां चीन में सैनिक शक्ति का पर्याप्त संचय हो सका था, वहां भारत में गाँधी जी के शिष्य जवाहरलाल अपने सैनिकों के हाथ में आटोमैटिक राइफल भी नहीं दे सके।
‘‘वर्तमान दुर्व्यवस्था का बीजारोपण तो सन् १९१६ और १९२१ में ही हुआ है। सन् १९१६ में मुसलमानों के विशेषाधिकार स्वीकार करके और सन् १९२१ में शासन से हिन्दू समाज के बुद्धिशील घटकों को पृथक् रखकर।’’
‘‘हां! मैं समझता हूं कि तुम्हारा विश्लेषण ठीक ही है। जैसे पाकिस्तान बनना भारत रोक नहीं सका, वैसे ही चीन की विजय अवश्ययंभावी है।’’
‘‘एक ही आशा की किरण दिखायी देती है। यू० के० सरकार इस संघर्ष में रुचि ले रही प्रतीत होती है। कदाचित् वह देखना चाहती है कि भारत स्वतः चीन के आक्रमण का विरोध कर सकेगा अथवा नहीं। मैं इसका अर्थ यह समझा हूं कि यू० के० सरकार चीन का भारत भूमि पर विजय पसन्द नहीं करेगी।
‘‘सबसे बड़ी बात है बंगाल की खाड़ी में चीन का पहुंचना। इससे यू. के. के अपने हितों को भय उत्पन्न हो जायेगा।’’
तेजकृष्ण नज़ीर को, राजनीति के विषय में इस प्रकार युक्ति करते देख चकित भी था और प्रसन्न भी।
|
|||||


 i
i