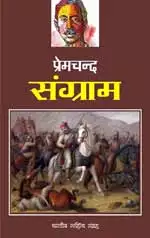|
नाटक-एकाँकी >> संग्राम (नाटक) संग्राम (नाटक)प्रेमचन्द
|
269 पाठक हैं |
मुंशी प्रेमचन्द्र द्वारा आज की सामाजिक कुरीतियों पर एक करारी चोट
ज्ञानी– कपड़े तो साधारण ही पहन कर गये हैं, पर कमरा न जाने क्यों भांय-भांय कर रहा है, वहां खड़े होते एक भय-सा लगता था। ऐसी शंका होती है कि वह अपनी मसनद पर बैठे हुए हैं पर दिखायी नहीं देते। न जाने क्यों मेरे तो रोयें खड़े हो गये और रोना आ गया। किसी को भेज कर पता लगवाइये।
[सबल दोनों हाथों से मुंह छिपाकर रोने लगता है।]
ज्ञानी– हांय, यह आप क्या करते हैं! इस तरह जी छोटा न कीजिये। वह अबोध बालक थोड़े ही है। आते ही होंगे।
सबल– रोते हुए आह ज्ञानी! अब वह घर न आयेंगे। अब हम उनका मुंह फिर न देखेंगे।
ज्ञानी– किसी ने कोई बुरी खबर कही है क्या? (सिसकियां लेती है।)
सबल– (मन में) अब मन में बात नहीं रह सकती। किसी तरह नहीं। वह आप ही बाहर निकली पड़ती है। ज्ञानी से मुझे इतना प्रेम कभी न हुआ था। मेरा मन उसकी ओर खिंचा जाता है। (प्रकट) जो कुछ किया है मैंने ही किया। मैं ही विष की गांठ हूं। मैंने ईर्ष्या के वंश होकर यह अनर्थ किया है। ज्ञानी मैं पापी हूं, राक्षस हूं, मेरे हाथ अपने भाई के खून से रंगे हुए हैं, मेरे सिर पर भाई का खून सवार है। मेरी आत्मा की जगह अब केवल कालिमा की रेखा है! हृदय के स्थान पर केवल पैशाचिक निर्दयता। मैंने तुम्हारे साथ दगा की है। तुम और सारा संसार मुझे एक विचारशील, उदार, पुण्यात्मा पुरुष समझता था, पर मैं महान पापी, नराधम, धूर्त हूं। मैंने अपने असली स्वरूप को सदैव तुमसे छिपाया। देवता के रूप में मैं राक्षस था। मैं तुम्हारा पति बनने योग्य न था। मैंने एक पति परायणा स्त्री को कपट चालों से निकाला, उसे लाकर शहर में रखा। कंचनसिंह को भी मैंने वहां दो-तीन बार बैठे देखा। बस, उसी क्षण में ईर्ष्या की आग में जलने लगा और अंत में मैंने एक हत्यारे के हाथों...(रो कर) भैया को कैसे पाऊं? ज्ञानी, इन तिरस्कार के नेत्रों से न देखो। मैं ईश्वर से कहता हूं तुम कल मेरा मुंह न देखोगी। मैं अपनी आत्मा को कलुषित करने के लिए अब और नहीं जीना चाहता। मैं अपने पापों का प्रायश्चित्त एक ही दिन में समाप्त कर दूंगा। मैंने तुम्हारे साथ दगा की, क्षमा करना।
ज्ञानी– (मन में) भगवन् पुरुष इतने ईर्ष्यालु, इतने विश्वासघाती, इतने क्रूर, वज्र-हृदय होते हैं! आह! अगर मैंने स्वामी चेतनदास की बात पर विश्वास किया होता तो यह नौबत न आने पाती। पर मैंने तो उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। यह उसी अश्रद्धा का दंड है। (प्रकट) मैं आपको इससे ज्यादा विचारशील समझती थी। किसी दूसरे के मुंह से ये बातें सुनकर विश्वास न करती।
सबल– ज्ञानी, मुझे सच्चे दिल से क्षमा करो। मैं स्वयं इतना दुःखी हूं कि उस पर एक जौ का बोझ भी मेरी कमर तोड़ देगा। मेरी बुद्धि इस समय भ्रष्ट हो गयी है। न जाने क्या कर बैठूं। मैं आपे में नहीं हूं। तरह-तरह के आवेग मन में उठते हैं। मुझमें उनको दबाने की सामर्थ्य नहीं है। वचन के नाम से एक धर्मशाला और ठाकुर द्धारा अवश्य बनवाना। मैं तुमसे यह अनुरोध करता हूं। यह जल्द समाप्त होने वाला है। कंचन की यह जीवन-लालसा थी। इन्हीं लालसाओं पर उसने जीवन के सब आनंदों, सभी पार्थिव सुखों को अर्पण कर दिया था। अपनी लालसाओं को पूरा होते देखकर उसकी आत्मा प्रसन्न होगी और इस कुटिल निर्दय आघात को क्षमा कर देगी।
[अचलसिंह का प्रवेश]
|
|||||


 i
i