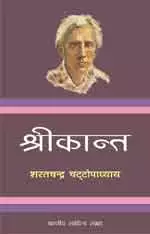|
उपन्यास >> श्रीकान्त श्रीकान्तशरत चन्द्र चट्टोपाध्याय
|
337 पाठक हैं |
शरतचन्द्र का आत्मकथात्मक उपन्यास
रतन आकर हुक्का ले गया। बाईजी बोलीं, “आप तमाखू पीते हैं, यह मैं जानती हूँ; किन्तु दूँ किस तरह? और जगह आप चाहे जो करें, किन्तु मैं जान-बूझकर तो आपको अपना हुक्का दे न सकूँगी। अच्छा, चुरुट लाए देती हूँ। अरे ओ...”
“ठहरो, ठहरो, जरूरत नहीं। मेरी जेब में चुरुट हैं।”
“हैं? अच्छा तो ठण्डे होकर जरा बैठ जाइए, बहुत-सी बातें करनी हैं। भगवान कब किससे मिला देते हैं, सो कोई नहीं कह सकता, यह स्वप्न में भी अगोचर है। शिकार के लिए गये थे, एकाएक लौट क्यों आए?”
“तबीयत न लगी।”
“न लगने की ही बात है। कैसी निष्ठुर है यह पुरुषों की जात। निरर्थक जीव-हत्या करने में इन्हें क्या मजा आता है सो ये ही जानें। बाबूजी तो अच्छे हैं न?”
“बाबूजी का स्वर्गवास हो गया।”
“हैं, स्वर्गवास हो गया! और माँ?”
“वे तो उनसे भी पहले चल बसी थीं।”
“ओह-तभी तो!” कहकर बाईजी एक दीर्घ नि:श्वास छोड़कर मेरी ओर देखती रह गयीं। एक दफा तो जान पड़ा मानो उनकी आँखें छलछला आयीं हैं, किन्तु, शायद वह मेरी भूल हो। परन्तु, दूसरे ही क्षण जब वे बोलीं तब भूल के लिए कोई जगह न रही। उस मुखरा नारी का चंचल और परिहास लघु कण्ठस्वर सचमुच ही मृदु और आर्द्र हो उठा था। बोलीं, “तो फिर यों कहो कि अब तुम्हारा जतन करने वाला कोई न रहा। बुआजी के पास ही रहते हो न? नहीं तो, और फिर कहाँ रहोगे? ब्याह हुआ नहीं, यह तो मैं देख ही रही हूँ। पढ़ते-लिखते हो? या वह भी इसके साथ ही समाप्त कर दिया?”
|
|||||


 i
i