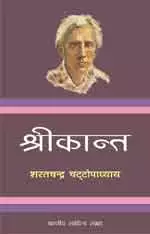|
उपन्यास >> श्रीकान्त श्रीकान्तशरत चन्द्र चट्टोपाध्याय
|
337 पाठक हैं |
शरतचन्द्र का आत्मकथात्मक उपन्यास
2
पैर उठते ही न थे, फिर भी किसी तरह गंगा के किनारे-किनारे चलकर सवेरे लाल आँखें और अत्यन्त सूखा म्लान मुँह लेकर घर पहुँचा। मानो एक समारोह-सा हो उठा। “यह आया! यह आया!” कहकर सबके सब एक साथ एक स्वर में इस तरह अभ्यर्थना कर उठे कि मेरा हृत्पिण्ड थम जाने की तैयारी करने लगा।
जतीन करीब-करीब मेरी ही उम्र का था। इसलिए आनन्द भी उसका सबसे प्रचण्ड था। वह कहीं से दौड़ता हुआ आया और “आ गया श्रीकान्त - यह आ गया, मँझले भइया!” इस प्रकार के उन्मत्त चीत्कार से घर को फाड़ता हुआ मेरे आने की बात घोषित करने लगा और मुहूर्त भर का भी विलम्ब किये बगैर, उसने परम आदर से मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए मुझे बैठकखाने के पायंदाज पर ला खड़ा किया।
वहाँ पर मँझले भइया गहरा मन लगाए परीक्षा पास करने का पाठ पढ़ रहे थे। मुँह उठाकर थोड़ी-सी देर मेरे मुँह की ओर देखकर उन्होंने फिर पढ़ने में अपना मन लगा दिया अर्थात् बाघ, शिकार को अपने अधिकार में कर लेने के उपरान्त, निरापद स्थान में बैठकर, जिस तरह दूसरी तरफ अवहेलना भरी दृष्टि से देखता है, ठीक उसी तरह उनका भाव था। दण्ड देने का इतना बड़ा महेन्द्र योग उनके भाग्य में पहले और कभी जुटा था या नहीं, इसमें सन्देह है।
मिनट-भर वे चुप रहे। सारी रात बाहर बिताने के कारण दोनों कानों और गालों पर जो कुछ बीतेगी सो मैं जानता था। किन्तु, अब और अधिक देर खड़ा भी न रह सकता था और उधर 'कर्म-कर्ता' को भी तो फुरसत नहीं थी। वे भी तो परीक्षा पास करने की तैयारी में लगे थे!
|
|||||


 i
i