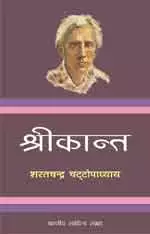|
उपन्यास >> श्रीकान्त श्रीकान्तशरत चन्द्र चट्टोपाध्याय
|
337 पाठक हैं |
शरतचन्द्र का आत्मकथात्मक उपन्यास
इतने दिनों बाद पहले-पहल आज उन्होंने कहा कि शाहजी उनका पति था किन्तु, इन्द्र के मन में यह बात अच्छी तरह जमकर बैठती ही नहीं थी। संदिग्ध स्वर से उसने प्रश्न किया, “किन्तु तुम तो हिन्दू की लड़की हो जीजी?”
जीजी बोली, “हाँ, ब्राह्मण की लड़की हूँ और वे भी ब्राह्मण थे।”
इन्द्र कुछ देर अवाक् हो रहा, फिर बोला, “उन्होंने अपनी जात क्यों छोड़ दी?”
जीजी बोली, “सो बात मैं अच्छी तरह नहीं जानती भाई। किन्तु जब उन्होंने अपनी जात खो दी, तो उसके साथ मेरी भी खो गयी। स्त्री सहधर्मिणी जो है! नहीं तो वैसे मैंने अपने हाथों अपनी जाति भी नहीं छोड़ी- और किसी दिन किसी तरह का अनाचार भी नहीं किया।”
इन्द्र गाढ़े स्वर में बोला, “सो तो मैं देखता हूँ जीजी! इसीलिए तो जब तब मेरे मन में यही बात आती रही है, मुझे माफ करना जीजी - तुम कैसे यहाँ आ पड़ीं, तुम्हारी किस तरह ऐसी दुर्बुद्धि हुई। परन्तु अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूँगा, मेरे घर तुम्हें चलना ही पड़ेगा। चलो, इसी वक्त चलो।”
जीजी देर तक चुपचाप मानो कुछ सोचती रहीं, फिर मुँह उठाकर धीरे-धीरे बोलीं, “अभी मैं कहीं भी जा न सकूँगी, इन्द्रनाथ।”
“क्यों नहीं जा सकोगी जीजी?”
जीजी बोलीं, “मुझे मालूम है कि वे कुछ 'देना' कर गये हैं। जब तक उसे चुका न दूँ, तब तक मैं कहीं हिल नहीं सकती।”
|
|||||


 i
i